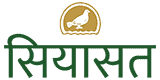यह एक ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आसानी से ज्ञात नहीं किया जाता है, इस प्रकार शायद ही कभी यह स्वीकार किया जाता है कि एक समय में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक परियोजना भारत के विच्छेदों की खुदाई में बदल गई थी। इस खुदाई का उद्देश्य उपमहाद्वीप में विभिन्न विदेशी लोगों, संस्कृतियों, धर्मों और राजनीति के आगमन की खोज करना था।
आखिरकार, भारतीय प्रायद्वीप 1498 के बाद से पोर्तुगीज, डच और टिमूरिड्स द्वारा वाणिज्यिक, राजनीतिक और सैन्य घुसपैठ की जगह थी। निश्चित रूप से, खुदाई का एक कारण यह था कि, भारत में आने वाले नवीनतम विदेशियों के रूप में, ब्रिटिश अपने आगमन के लिए एक औचित्य चाहता था अन्य कारण जिस तरह से अंग्रेजों ने खुद को रोमियों के वारिस के रूप में देखा था, उससे जुड़ा हुआ है।
एडवर्ड गिब्बन ने 1776 में द रोमन साम्राज्य का इतिहास और उसकी गिरावट का इतिहास प्रकाशित किया, द ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका में अपनी 13 कॉलोनियों को खो दिया। किताब के सभी छह खंडों को 1788 तक भारी प्रशंसा और बिक्री मिली। गिब्बन के काम का एक केंद्रीय विषय, उनकी ब्रिटिश पब्लिक ब्रिटैनिका के बीच ऐतिहासिक संबंधों की खोज थी- ब्रिटिश-प्रभुत्व वाले विश्व व्यवस्था की अवधि- और पैक्स रोमाना.
उन्होंने एक सिद्धांत के लिए आधारभूत पत्थर प्रदान किया जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक उद्यम को अतीत के एक महान साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में वैध बनाने की मांग की, जो यूरोप के लिए शांति और समृद्धि के लंबे युग में पैदा हुआ था। इससे भी अधिक प्रभावशाली, मैं बहस करता हूं, वह रोमन अनुभव के संदर्भ में जाति और राजनीति के बीच के संबंधों की खोज करना है। इस रिश्ते को तत्काल भारत के ब्रिटिश विजय को वैध बनाने में नियोजित किया गया था.
विद्वान योद्धाओं की श्रृंखला
प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश औपचारिक रूप से 1757 में भारत में अपनी शाही परियोजना शुरू हुई. 1783 में, विलियम जोन्स कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सत्र न्यायाधीश के रूप में पहुंचे। अगले दशक में, उन्होंने भाषा विज्ञान के नए विज्ञान की स्थापना की, जिसमें मानव प्रवास पैटर्न के साथ संयुक्त भाषा विज्ञान और इंडो-यूरोपियन क्षेत्र में दौड़ के मिंगलिंग शामिल थे। उन्होंने प्राचीन भाषाओं और प्रागैतिहासिक माइग्रेशन को भारत में विदेशी आगमन के लंबे इतिहास के साथ जोड़ा, एक ऐसी प्रक्रिया जो उपमहाद्वीप में ब्रिटिश उपस्थिति के आगमन में समाप्त हो जाएगी। वह एक ऐसी कहानी के साथ आया जो यूनानी, लैटिन और संस्कृत भाषाओं को एक “सामान्य स्रोत” के माध्यम से जोड़ती है जो “अब अस्तित्व में नहीं है” यह “आम स्रोत” कुछ बहुत ही दूरदराज के युग में “अन्य राज्यों के विजेता” था।
19वीं शताब्दी की शुरुआत में, ब्रिटिश अधिकारियों की एक नई पीढ़ी भारत के विद्वानों के विद्वान बन गई। वे खुद को बाद के अलेक्जेंडर ग्रेट्स के रूप में सोच रहे थे, भौगोलिक, लोक और वस्तुएं जो कि भारत को यूनानियों से जोड़ता है, और अतीत की रोमनों के विस्तार से संबंधित है। अलेक्जेंडर बर्नेस, जेम्स टॉड, रिचर्ड एफ बर्टन और एडवर्ड बी ईस्टविक उनके बीच सबसे प्रमुख थे।
उपमहाद्वीप के उत्तरी-पश्चिमी हिस्सों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने सिकंदर के माध्यम से ग्रीक प्रभाव के माध्यम से भारत कैसे स्थापित किया, यह स्थापित करने के लिए उन्होंने काबुल और बॉम्बे के बीच यात्रा की और पांडुलिपियों, सिक्कों और तांबे के बर्तनों के बीच कूच किया। उनका शोध भारत के साथ ग्रीक और रोमन व्यापार पर केंद्रित है, अलेक्जेंडर की विजय और उनकी सेनाओं के अवशेष जो उन क्षेत्रों में रहे जहां से वे पास गए थे।
उन्होंने उपमहाद्वीप में मध्य एशियाई स्टेप से माइग्रेशन और भाषाओं, शहरों, धर्मों और राजनीति के विकास के लिए इन सभी घटनाओं का संबंध भी देखा। बंगाल और बॉम्बे के शाही एशियाई समाजों के पत्रिकाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य, इंडो-पार्थियन, इंडो-बैक्ट्रीयन और “व्हाईट हून” की उपस्थिति पर अपने शोध प्रकाशित किए – समुदायों, जो एक सामान्य यूरेशियन वंश के संकेत थे।
19वीं शताब्दी के मध्य तक, ब्रिटिश इतिहासकारों की एक नई पीढ़ी ने इस कच्चे डेटा को ऐतिहासिक ग्रंथों में सम्मिलित करने का प्रोजेक्ट उठाया। एचएम इलियट और एम एलफिंस्टोन इस पीढ़ी के अग्रदूत थे। इसके बाद विन्सेंट स्मिथ, स्टेनली लेन-पोले, अलेक्जेंडर कनिंघम और आरबी व्हाइटहेड, उनके अलावा अन्य शामिल थे जैसा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक परियोजना ने भौगोलिक दृष्टि से – कलकत्ता से दिल्ली तक, मद्रास से बॉम्बे और लाहौर से पेशावर तक विस्तार किया – यह समय तक गहरा और गहरा हो गया जब तक भारत के विच्छेदों की खुदाई का संबंध था।
संस्कृत भाषा की जड़, आर्यन वंश की वंशावली, उपमहाद्वीप के “स्वदेशी जनजातियों” की उत्पत्ति और स्थानों के नामों की व्युत्पत्तियां औपनिवेशिक भाषण, जर्नल लेख, ट्रैवेलोगेज, जिला रिपोर्ट, इतिहास के विशाल रकम में नियमित रूप से दिखाई देती हैं और उस युग की टिप्पणियां इस परियोजना के मध्य में बसे – और पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में हाइलाइट किया गया – भारत में मुस्लिम आगमन का सवाल है।
पुरानी गलत बातें ठीक करना
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1843 में तायनपुर मिरियस को मियान में हराया और सिंध की रियासत पर कब्जा कर लिया। विजय भारत के मुस्लिम विजय के लिए सुधारात्मकता के रूप में डाली गई – 8वीं शताब्दी की शुरुआत के रूप में वापस जाने वाले विदेशी मुस्लिम शासन के चंगुल से हिंदुओं को मुक्त करने की एक चाल थी। सिंधु नदी अरबी सागर में खोलने के डेल्टा पर केंद्रित, सिंध में कई पत्तियां और सूखी, रेगिस्तान जैसे इलाके के बड़े इलाके शामिल थे।
19वीं शताब्दी की शुरुआत में राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सीमावर्ती इलाका था, हालांकि समकालीन मानचित्रों में यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब और बलूचिस्तान जैसे उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों से घिरा हुआ है। तब तक कंपनी द्वारा अविवाहित सिंधु ने रणजीत सिंह के सिख राज्य की राजधानी मुंबई से लाहौर तक एक नदी के ऊपर की तरफ लिंक की पेशकश की थी। थार और बलूचिस्तान के रेगिस्तान के माध्यम से, सिंध ने भारत को काबुल में दुर्रानी अदालत में जोड़ा।
कंपनी ने इसे अपने लंबे समय से स्थापित बॉम्बे प्रेसीडेंसी और अफगानिस्तान (साथ ही मध्य एशिया और ईरान में फ्रांसीसी और रूसी हितों) के बीच एक आवश्यक बफर के रूप में सोचा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके विद्वान-योद्धाओं ने पहले ही पता लगाया था कि यह सिंध में था कि मुहम्मद बिन कसीम ने “व्हाइट हंट” द्वारा स्थापित राज्य को हरा दिया था- 712 में भारत के हिंदुओं को एक सहस्राब्दी में धकेल दिया था। मुसलमानों का वर्चस्व इस खोज को तुरंत राजनीतिक उपयोग के लिए रखा गया था।
उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर-जनरल एडवर्ड लॉ एलनबोरो ने नाटकीय रूप से काबुल के “सोमनाथ के द्वार” को वापस हिंदुओं को दिखाने के लिए भेजा था कि उनकी कंपनी मुस्लिम आतंकियों का मुकाबला करने के लिए वहां थी। 1842 के अपने “सभी राजकुमारों और प्रमुखों और भारत के लोगों” के घोषणापत्र में, उन्होंने घोषणा की कि भारत के मंदिरों के खराब अवशेषों की वापसी ने “800 साल का अपमान … सोमनाथ मंदिर के द्वार, का बदला लिया” लंबे समय तक अपने अपमान के स्मारक, आपके राष्ट्रीय गौरव का सबसे गर्ववादी रिकॉर्ड बन गए हैं”। एलनबोरो की राजनीतिक रणनीति थी कि हिंदुओं पर मुस्लिमों द्वारा किए गए ऐतिहासिक नुकसान की शुद्धता के रूप में कंपनी को डालना। यह थोड़ा मायने रखता है कि “द्वार” को सोमनाथ के साथ कुछ नहीं करना था.
चार्ल्स नेपियर, यूरोप में शाही युद्ध के एक अनुभवी सैन्य कमांडर थे जिन्हें सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए एलनबोरो द्वारा चुना गया था, वह एक गंभीर धार्मिक व्यक्ति था। सिंध में अपना अभियान शुरू करने के बाद वह अभी भारत आए थे।
उन्हें विश्वास था कि कंपनी वाणिज्य के लिए आभारी हो गई थी और अपने दिव्य मिशन से दूर हो गई थी। उन्होंने अपने ईसाई कर्तव्य के रूप में अपने निंदनीय मुस्लिम शासकों से सिंध की कथित मुक्ति को देखा. उन्होंने तालपुर को “महान रुफ्फियन” और “इम्बेसिलेस” कहा जाता है, जो “अपने दोस्तों से फटे युवा लड़कियों से भरा जनेना” और “क्रूर जंगलीपन के साथ” महिलाओं को हरम में समझाते थे। उन्होंने कहा, तालपुर, कभी कभी “मानव त्याग” का आनंद लेने के लिए प्रवण थे.
17 फरवरी, 1843 को नेपियर के सिंध के कब्जे को ब्रिटिश ने एक वीर घटना के रूप में स्वागत किया। उनमें से कुछ ने इसे प्लासी की लड़ाई के साथ तुलना की, भारत में ब्रिटिश शासन के संस्थापक पल. एक ने लिखा, “प्लासी में क्लाइव की शानदार जीत से भारत में देशी या यूरोपीय सैनिकों के साथ तुलना करने के लिए कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।” यह उनकी जीत में था कि भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के बारे में कहानियां – लंबे समय से विस्थापित और वर्चस्व वाले भारत-यूरोपीय दौड़ की वापसी के रूप में चित्रित की गईं- और उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की उत्पत्ति के बारे में उनको एक विदेशी धार्मिक शक्ति, समन्वित की गयी.
भारत में मुस्लिम मूल के लिए ब्रिटिश खोज ने बाद में कलकत्ता, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के बड़ौदा और उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित देशी इतिहासकारों की ऐतिहासिक चेतना को आकार दिया। शिबली नोमनी (1857-1914), जुडुननाथ सरकार (1870-1958), सैयद सुलेमान नदवी (1884-1953), आर.सी. मजूमदार (1888-1980), मोहम्मद हबीब (1895-1971) और बी.डी. मीरचंदानी (1906-1980) कुछ हैं जो उप इतिहास में मुसलमानों के आगमन के सवाल से जूझ रहे प्रमुख इतिहासकारों में से वे औपनिवेशिक इतिहास-विज्ञान के प्रति एक राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया ढूंढने का प्रयास करते थे।
पत्रिकाओं में लेखन जैसे कि कलकत्ता रिव्यू, मुस्लिम रिव्यू, इस्लामिक कल्चर और इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू, उनमें से कई ने औपनिवेशिक इतिहास में भारत में मुस्लिम शासन के बारे में औपनिवेशिक कथाओं के साथ संघर्ष करने का प्रयास किया। उन्होंने मुस्लिम इतिहास को एक राष्ट्रवादी कथा में बुनाई करने के लिए संघर्ष किया, यह देखते हुए कि उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासकों को औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा विदेशी मूल के तानाशाह के रूप में दिखाया गया था जिन्होंने अपने विजय और शासन के दौरान अनगिनत हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था।
भारत में मुसलमानों के बारे में बहस के मध्य में धार्मिक आक्रमणकारियों के बाहर एक विशिष्ट पाठ था – चचनामा यह बीट्स और टुकड़ों में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में औपनिवेशिक इतिहास लेखन में दर्ज किया गया था। इलियट से एल्फिन्स्टन और स्मिथ, भारत में इस्लाम के इतिहास पर लिखते हुए ब्रिटिश इतिहासकारों ने चचननाम को विजय की पुस्तक के रूप में इलाज किया। मूलतः 1220 के आसपास फारसी में लिखा गया, यह सिंध में मुहम्मद बिन कासिम के अभियान की 8 वीं शताब्दी के अरबी इतिहास का स्वयं-अनुवादित अनुवाद था। यह उन घटनाओं का वर्णन करता है जो उनकी विजय से पहले और जो कि दुनिया के इस हिस्से में रहने के दौरान हुआ था – लगभग 60 वर्षों से अधिक समय तक फैली अवधि थी।
सरकार और मजूमदार जैसे भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लेखन में, चचननाम और बाहरी मुस्लिम का आंकड़ा बड़े पैमाने पर उभर रहा था भारतीय पट्टों पर सरकार के व्याख्यानों के साथ-साथ मुगल भारत के इतिहास ने ब्रिटिश इतिहासकारों से अपनी राय ली और तर्क दिया कि “विदेशी आप्रवासी” मुसलमानों द्वारा भारत की विजय ने मूल रूप से सभी पूर्ववर्ती आक्रमणों से इस्लाम के “घनिष्ठ एकतावादी प्रकृति” की वजह से मतभेद किया – जो कुछ विपरीत है ईसा पूर्व इस्लाम के बहुदेववादी धार्मिक अभ्यासों के साथ “अरब विजय” सिंध के मजूमदार के उपचार ने मुसलमानों को स्वभाव से विजेता प्रस्तुत किया जिन्होंने स्पेन पर विजय प्राप्त करने के बाद अनिवार्य रूप से भारत पर अपनी लालची आंखें डालीं।
सैटलर्स, विजेता नहीं
इसके विपरीत, मुस्लिम विद्वानों की एक पीढ़ी ने अरब और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया, जो मुहम्मद बिन कासिम के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। नोमनी ने उन कनेक्शनों को इस्लाम के पैगंबर और उनके प्रारंभिक इस्लाम के अन्य प्रमुख आत्मकथाओं के जीवनचिकित्सा में प्रकाश डाला। 1882 और 1898 के बीच, उन्होंने भारत के शुरुआती मुस्लिम राज्य की एक विस्तृत विविधता के निबंध का निर्माण किया, जिसमें दोनों क्षेत्रों के बीच सबसे प्रारंभिक संबंधों को उजागर किया गया था। नदवी और अब्दुल हलीम शारार ने 20 वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में एक ही नस में सिंध के इतिहास को लिखा। हबीब, एक मार्क्सवादी इतिहासकार, अपने 1929 के निबंध अरब विजय के सिवा में बलपूर्वक तर्क दिया कि मुसलमान भारत में विजयी नहीं हुए बल्कि बसने के रूप में आ रहे थे।
हालांकि, इन मुस्लिम इतिहासकारों ने विजय की पुस्तक के रूप में चचननाम के वर्गीकरण का अंदाजा नहीं किया। 1947 के बाद भी, दक्षिण एशिया और यूनाइटेड किंगडम में काम करने वाले इतिहासकारों ने सिंध में मुस्लिम पट्टों के इतिहास में और जांच की है, जिसने इस प्राचीन पाठ को जिस तरह से औपनिवेशिक इतिहासकारों ने किया था, उसका इलाज किया। उम दोडपोता, नबी बुख्श खान बलोच, मुबारक अली, एच.टी. लमब्रिक और पीटर हार्डी ने सभी चीखनाम पर कई लेख और पुस्तकें लिखी हैं। वे सभी सहमत हैं कि सिंध के मुहम्मद बिन कसीम द्वारा सैन्य विजय ने भारत में मुस्लिम आगमन की शुरुआत की।
फिर भी यह उत्पत्ति कथा चचननाम के गलत वर्गीकरण पर आधारित थी। यह उस समय के अरबी या फारसी में लिखे गए किसी भी अन्य इतिहास के विपरीत नहीं पढ़ता है। इसमें मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण और सिंध का कब्ज़ा करने के लिए बहुत कुछ प्रासंगिक है। यह कम से कम 8 वीं शताब्दी का इतिहास है और 13 वीं शताब्दी के लिए एक राजनीतिक सिद्धांत अधिक है। इसका एक अरबी पाठ का अनुवाद होने का दावा है, वास्तव में, सिंध के लगभग 500 वर्षों की मुस्लिम उपस्थिति को सहवास और आवास के युग के रूप में याद करने का मतलब है।
यह सिंध और गुजरात में बंदरगाहों जैसे दीबुल, दीव और ठाणे – और एडन, मस्कट, बहरीन, दमम और सिरफ के अरब बंदरगाहों के बीच दोनों भूमि और समुद्र के संबंधों का एक इतिहास प्रदान करता है। यह फारसी, पहलवी और प्राकृत में ग्रंथों पर आधारित है जो एक ओर ओमान और यमन के बीच हजारों साल के कनेक्शन और दूसरी तरफ श्रीलंका और जंजीबार का पता लगाता है। चचनाम में, ये संबंध व्यापार, विवाह, निपटान, भाषा और रीति-रिवाजों का विस्तार करते हैं और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच विरोधाभास बनाने और बनाए रखने में असंभव बना देते हैं, केवल प्रतिद्वंद्वियों के रूप में।
1820 के शुरुआती दौर से ही ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा इस पुस्तक को जानबूझकर दुरूपयोग किया गया और गलत तरीके से पढ़ लिया गया। उन्होंने अपने कार्य में “अन्य” को “बाहरी” के साथ बदल दिया और संबंधित होने का इतिहास बहिष्कार का इतिहास बन गया।
इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड
जॉन जहांगीर बेडे की डॉक्टरेट निबंध, सिंध में अरब: 712-1026 एडी, इस शैक्षणिक संदर्भ में लिखा गया था। 1973 में यूटा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया था, सिंध के विरासत के संरक्षण के लिए कराची एंडॉमेंट फंड ट्रस्ट के लिए इस वर्ष की शुरुआत में इसे प्रकाशित नहीं किया गया था।
हमें नहीं पता कि बेडे ने अपने काम को कभी क्यों नहीं प्रकाशित किया पुस्तक राज्य की धूल जैकेट पर टिप्पणी करते हुए कि उनके परिवार या कैरियर का पता लगाने के सभी प्रयास बड़े पैमाने पर असफल रहे थे। केवल एक चीज है जो हमें पता है कि उन्होंने क्रूसेड के एक प्रभावशाली इतिहासकार डॉ अजीज एस अट्टिया के साथ काम किया है और उनके काम का उल्लेख इतिहासकारों जैसे डेरेली मैकलेन, मुबारक अली, मुहम्मद यार खान और योहन फ्रिडमैन ने किया है। 1980 और 1990 के दशक 2017 में हम इस शोध प्रबंध को कैसे पढ़ सकते हैं? एक संभव तरीका यह है कि भारत में मुस्लिम मूल के इतिहास के साथ-साथ, ऊपर वर्णित इतिहासलेखन, 1973 की तरह देखा गया।
सिंध के इतिहास को थोड़ा समकालीन ध्यान मिला है, इस तथ्य पर प्रतिबिंबित करके बेडे अपने शोध प्रबंध शुरू करता है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इतिहास के लिए अपेक्षाकृत कम पाठ्य स्रोत हैं और इतिहासकार “आम तौर पर पूर्वकेंद्रित पूर्वाग्रहों के अधीन हैं, जो मुख्यतः विशेष लेखकों के धार्मिक दृष्टिकोण से रंगे हैं”।
मुसलमानों को धार्मिक आक्रमणकारियों के इलाज के बजाय, उन्होंने विभिन्न स्रोतों की जांच करके सिंध की विजय के लिए एक आर्थिक आधार की खोज की, जो कि 9वीं शताब्दी के मध्य तक की तारीख का सबसे पुराना था। सिंध में वाणिज्य और संस्कृति के अपने आखिरी अध्याय में, वह 9वीं और 10वीं शताब्दियों से यात्रा, व्यापारिक खातों और कविताओं पर विचार करने के लिए आकर्षित होते हैं कि वहां एक बार एक दूसरे से जुड़े हिंद महासागर की दुनिया में मौजूद थे जिसमें सिंध एक धुरी थी।
बेडे ने औपनिवेशिक ऐतिहासिक कथा को भी बदनाम किया जो कि भारत में ब्रिटिश आगमन उपमहाद्वीप में मुस्लिम आगमन से पूरी तरह भिन्न था। उन्होंने कहा कि सिंध के अरब विजय का इतिहास 1843 में अपने ब्रिटिश विजय के इतिहास के समान है। “… एक हजार साल बाद भारत में सिंध के अरब प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासन के बीच एक समान समानता है” वह टिप्पणी करते हैं!
बेडे का काम हमारी दुनिया को एक कलाकृति या वस्तु के रूप में प्रवेश करता है यह जरूरी है – इतिहास लेखन के पहले के युग में एक फ्रोजन नमूना। इसकी जड़ता हमें सिंध के विरासत के संरक्षण के लिए कराची एंडॉवमेंट फंड ट्रस्ट को देखने के लिए प्रेरित करती है, जिसने इस वस्तु को दुनिया में लाया है। ईएफ़टी एक गैर लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन है जो सिंध की “कलात्मक, मूर्त और अमूर्त विरासत” को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। ऐसा लगता है कि सिंध में विभिन्न पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, रखरखाव और संरक्षण में अच्छे काम किए जा रहे हैं।
यह पुस्तक अपने प्रकाशन कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो नए कार्यों के लिए पुराने और अनुपलब्ध विद्वानों के लेखन को प्रकाशित करता है। हालांकि, मैं नए, अद्यतन, महत्वपूर्ण परिचय के बिना पुराने अनुदानों के पुन: प्रकाशन को एक अयोग्य सलाह के रूप में देखता हूं। यह विशेष रूप से बेडे के काम के लिए है, क्योंकि पहले अप्रकाशित किया जा रहा है, यह आवश्यक विद्वानों की समीक्षा और बहस के माध्यम से नहीं गया है। इस प्रकार, सिंध में अरब एक साधारण पाठक के लिए एक नया पाठ के रूप में प्रकट होता है जिसे सिंध पर छात्रवृत्ति के बारे में पता नहीं है या इसकी सामग्री कैसे समझनी है।
पुरानी ग्रंथों को प्रकाशित करने का अभ्यास पाकिस्तान में आम है; ब्रिटिश युग जिले के गजटेटर्स और अन्य औपनिवेशिक ग्रंथों को नियमित रूप से उपमहाद्वीप के इतिहास के वास्तविक तथ्यों के रूप में पुनर्मुद्रित किया गया है। इसका असर खराब होने पर यह है कि औपनिवेशिक पूर्वाग्रह और चौखटे बिना निर्विरोध और व्यापक रूप से लोकप्रिय रहते हैं। हमारे इतिहास को निराश करने का कोई भी प्रयास नहीं है और न ही हमारे पॉट्स के बारे में लिखने पर जो हिंसा से औपनिवेशिक ज्ञान प्रथाओं ने पलट ली है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
सिंध के अतीत को पुनर्विचार करना
विभाजन के 70 साल बाद, यह समय के बारे में है कि पाकिस्तान में पाठकों और लेखकों ने उनके इतिहास को फिर से और फिर से अनुमानित किया। अतीत की जरूरत है नए सवालों के प्रकाश में विश्लेषण और नए महत्वपूर्ण चौखटे। भारत में मुस्लिम आगमन के बारे में ब्रिटिश कथाओं को अरबों से धर्म-प्रेरित आक्रमणकारियों के रूप में हम बंधक नहीं बना सकते।
सिंध के अतीत को पुनर्विचार और पुन: विकसित करना – विशेषकर मोहनजोदड़ो से शुरू होने वाले युग के बारे में और मुहम्मद बिन कसीम के आगमन के अंत में – पाकिस्तान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि क्या हम किसी दिव्य मिशन पर बाहर आए हैं या हमारी कहानी अधिक है या नहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकारों की तुलना में जटिल, साथ ही साथ हमारे अपने राज्य-प्रायोजित इतिहास हैं, हमें विश्वास है।
हमें अपने इतिहास के प्राथमिक स्रोतों को विस्तारित करने की आवश्यकता है और बेडे के ग्रंथ इस गिनती पर उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। हमें संस्कृत, पहलवी, फारसी, अरबी, सिंधी और गुजराती जैसे भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जिसमें इन स्रोतों को लिखा गया था ताकि हम चाचमन के मामले में गलत तरीके से व्याख्या और गलत तरीके से व्याख्या नहीं करें। ये अध्ययन हमारे छात्रों को अपनी सभी जटिलताओं में मध्ययुगीन पट्टों को देखने के लिए सक्षम कर सकते हैं। हमें अपने संस्थानों को शोध और लेखन के नए तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी लैस करने की जरूरत है।
हमें ऐतिहासिक खातों में सूक्ष्मता और विविधता के विलोपन को रोकने के लिए इस सबका ज़रूरत है, औपनिवेशिक इतिहासलेखन के साथ शुरू हुआ एक अभ्यास और हमारे उत्तर-औपनिवेशिक उपस्थिति में जारी है। बेडे के निबंध में अंतिम फुटनोट इस विस्मरण के खिलाफ काम करने के लिए एक मजबूत तर्क प्रदान करता है।
यह नोट एक पैराग्राफ से संबंधित है जो “अरबों के उत्तराधिकारी” की प्रशंसा करता है, “जो कि खुद मुसलमानों, बुद्धिमानी से अपने गैर-मुस्लिम विषयों के प्रति एक सहिष्णु दृष्टिकोण बनाए रखते हैं”। बाद में क्या बदला गया, बेडे तर्क करता है, बाद के तुर्की शासकों का दृष्टिकोण था यह नोट ही हमें याद दिलाता है कि 1947 में “सिंध की पूरी आबादी का लगभग चौथा हिस्सा गैर-मुस्लिम था।” तब से इस अनुपात में कमी आई है। 1998 की जनगणना के अनुसार सिंध में हिंदू जनसंख्या लगभग 6% थी। यह हम सभी को परेशान करना चाहिए जो एक विविध पाकिस्तान की देखभाल करते हैं।
सिंध के अतीत को एक समुदाय, एक संप्रदाय या एक विश्वास के इतिहास में कम नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें इस प्रांत के साथ-साथ देश के लिए एक समावेशी उपस्थिति का लक्ष्य रखना चाहिए।
लेखक न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक इतिहासकार है।
यह आलेख पहले हेराल्ड में प्रकाशित हुआ था।