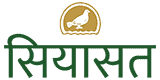केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और विकास की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि मानव स्वास्थ्य प्रर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साल 2030 तक भूमि क्षरण प्रक्रिया को पूरी तरह थामना बेहद जरूरी है। मरुस्थलीकरण की समस्या से निबटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) के तहत आज यहां आयोजित चार दिवसीय एशिया प्रशांत कार्यशाला का उद्घाटन करने के अवसर पर डॉ. हर्षवर्धन ने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वह इस कार्यशाला के जरिए भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे से निबटने के प्रभावी उपाय तलाशें।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में भूमि क्षरण का दायरा 96.40 मिलियन हेक्टेयर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.30 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि देश में प्रति मिनट 23 हेक्टेयर शुष्क भूमि सूखे और मरुस्थलीकरण की चपेट में आ जाती है जिसकी वजह से 20 मिलियन टन अनाज का संभावित उत्पादन प्रभावित होता है। संयुक्त राष्ट्र संधि की व्यवस्थाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश का 70 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र शुष्क भूमि के रूप में है जबकि 30 प्रतिशत जमीन भूक्षरण और 25 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजरती है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष करीब 24 अरब टन उपजाऊ मिट्टी और 27 हजार जैव प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की करीब 30 प्रतिशत आबादी शुष्क क्षेत्रों में रहती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 21 विश्व धरोहर स्थलों में से 8 शुष्क क्षेत्रों में है। भूक्षरण रोकने के लिए अन्य देशों द्वारा किये गए उपायों की सराहना करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने इस संदर्भ में बुरकिना फासो के साहेल एकीकृत समतल भूमि पारिस्थितिकी प्रबंधन तथा भूक्षरण और सूखे से निपटने में चीन की ओर से उसके यहां किये जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। भारत के संदर्भ में उन्होंने उत्तराखंड में आजीविका का स्तर सुधारने के लिए भूमि, जल और जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के उपायों को रेखांकित किया। उन्होंने भूमि और पारिस्थितिकी प्रबंधन क्षेत्र में नवाचार के जरिए टिकाऊ ग्रामीण आजीविका सुरक्षा हासिल करने के प्रयासों की सराहना की। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 2014 में प्रकाशित एसएलईएम पुस्तक भारत के टिकाऊ भूमि और पारिस्थितिकी प्रबंधन व्यवस्थाओं का दस्तावेज है।
केन्द्रीय मंत्री ने विभिन्न स्तरों पर हितधारकों के क्षमता विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, स्वच्छ भारत मिशन, हर खेत को पानी और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उल्लेख किया।
यूएनसीसीडी के उप कार्यकारी सचिव डॉ. पी. के. मोंगा ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यूएनसीसीडी से जुड़े देशों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उनके द्वारा भूक्षरण रोकने के उपायों की रिपोर्ट हासिल करना है। संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट कोऑर्डिनेटर श्री यूरी अफानासीव ने कहा कि भूमि क्षरण दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटा जा रहा है। भूक्षरण रोकने और ऊर्जा के किफायती इस्तेमाल के तरीके कम खर्चीले हैं।
इससे पहले डॉ. हर्षवर्धन ने उद्घाटन सत्र में ‘मरुस्थलीकरण का अर्थशास्त्र, भूक्षरण और सूखा’ शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया।
भारत में यह क्षेत्रीय कार्यशाला दुनिया भर में आयोजित यूएनसीसीडी कार्यशालाओं की श्रृंखला में चौथी है। इस चार दिवसीय कार्यशाला में (24-27 अप्रैल, 2018) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिनिधियों देश हिस्सा लेंगे। कार्यशाला में भारत के उन 12 राज्यों के प्रतिनिधियों को भूमि क्षरण की समस्या से निपटने में प्रशिक्षित किया जाएगा जिनके यहां इस समस्या की संभावना सबसे ज्यादा है। कार्यशाला में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश के प्रमुख वैज्ञानिक और शोध-आधारित संस्थानों के वैज्ञानिक और शिक्षाविद भी भाग ले रहे हैं।
मरुस्थलीकरण पर 1977 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पहली बार उपजाऊ भूमि के मरुस्थल में तब्दील होने की समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई थी। इसके बाद 17 जून 1994 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसके लिए बाकायदा एक वैश्विक संधि तैयार की गई जिसे दिसंबर 1996 में लागू किया गया। भारत 14 अक्टूबर 1994 को इस संधि में शामिल हुआ और 17 दिसंबर 1996 को उसने इसकी पुष्टि की। भारत के संदर्भ में संधि से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की प्रमुख जिम्मेदारी पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की है।