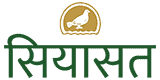‘पीड़ित सिर्फ़ पीड़ित होता है। उसका कारण जानने की ज़रूरत नहीं। जो लगातार प्रताड़ित हो रहा हो, वो पीड़ित है।’ -सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा,उन्मादी भीड़ मामले की सुनवाई पर
राष्ट्र सिहर उठा है कि हिंसक भीड़, संदेह जताकर लोगों को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार रही है। भीड़ का उन्माद भयंकर केवल इसीलिए होता है कि वह भीड़ है, उसकी कोई पहचान नहीं है। मॉब लिंचिंग की 25 से अधिक बर्बर वारदातों में, अफ़वाह फैलाने वाला माध्यम व्हॉट्सएप रहा है।
कोई 27 व्यक्तियों की ज़िंदगी लील चुकी ये अफवाहें व्हॉट्सएप पर षड्यंत्रपूर्वक चलाए गए, आपराधिक मैसेज थे। धैर्यपूर्वक, रुक-रुक कर, आधे-अधूरे और अलग-अलग आवाज़ों को इस्तेमाल किया गया। धीमे ज़हर की तरह। बरगलाया गया। झूठ फैलाया गया। उकसाया गया। किन्तु, ऐसा क्यों हो रहा है? या क्यों होने दिया जा रहा है?
हत्यारी भीड़ जैसा ही चरित्र है इन आपराधिक व्हॉट्सएप मैसेज़ेस का कि कोई पहचान नहीं। कहां से आया? किसने भेजा? सबसे पहले किस फोन, किस नंबर और किस जगह से जारी हुआ? कोई नहीं बता सकता। अभी महाराष्ट्र में भीड़ द्वारा 5 लोगों की हत्या के बाद साइबर क्राइम प्रमुख ब्रजेश सिंह ने ऐसी ही बेबसी जाहिर की। चूंकि अन्य मैसेजिंग एप्स की तरह व्हॉट्सएप नहीं है। वो मैसेज संभाल कर नहीं रखता। इसलिए तह में नहीं जा सकते। किन्तु यह तथ्य तो सभी जानते हैं।
जो कम पता है, वह महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कुछ ही नंबरों से, यानी सौ-पचास फोन या डिवाइस से, हजार-पांच सौ नंबरों को भेजे गए व्हॉट्सएप मैसेज पूरी ताकत से, सरलतापूर्वक पकड़े जा सकते हैं। कि कौन भेज रहा है। क्या भेज रहा है। किसे भेज रहा है। यानी अपराधी, अपराध, अपराध का मकसद सबकुछ पकड़ा जा सकता है।
उधर, केन्द्र सरकार का व्हॉट्सएप को लिखना और सुरक्षा के उपायों की जानकारी मांगना उचित कदम है। क्योंकि संभवत: हिंसा की एक भी घटना ऐसी नहीं है – जिसमें व्हॉट्सएप का प्रयोग न किया गया हो। किन्तु, व्हॉट्सएप का यह उत्तर कि ‘वह ‘हॉरिफाइड’ है’, कुछ समझ में नहीं आता। व्हॉट्सएप कंपनी बड़े छोटे-छोटे उपायों को बड़ा करके, बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है। वो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही मैसेज आगे बढ़ाने का अधिकार दे रही है।
किन्तु क्या ये एडमिन स्थानीय पुलिस थानों में पहचाने जा सकते हैं? यदि हां, क्योंकि फोन नंबर से सबकुछ पहचान हो सकती है – तो ग्रुप एडमिन बनने में निश्चित ही लोग डरने लगेंगे। या मैसेज संभलकर देखने लगेंगे। वो जिम्मेदार न होकर भी जिम्मेदार हो जाएंगे। बस, इसका कानूनी आधार बनाना होगा।
किन्तु दूसरा उपाय जो व्हॉट्सएप ने किया है – वो अधूरा है। भले ही महत्वपूर्ण हो। वो है, फॉरवर्ड मैसेज को ‘फॉरवर्ड’ लेबल करना। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि भेजने वाला ख़ुद इसे भेज रहा है – या उसे कहीं से मिला है। तो अफवाह, फेक न्यूज़, आपत्तिजनक कंटेन्ट या षड्यंत्रपूर्वक प्रचारित-प्रसाहित टैक्स्ट ऑडियो-वीडियो तत्काल पकड़े जा सकेंगे। महत्वपूर्ण व अपराधी को पकड़ने में उपयोगी होकर भी यह अधूरा कदम है।
पहली कमी है – भड़काने वाली सामग्री भेजने वाले पहले अलग-अलग स्मार्टफोन से इसे ख़ुद को भेजेंगे। फिर भेजेंगे तो उसे पाने वालों को ‘फॉरवर्ड’ के लेबल के साथ मिलेगा। किन्तु इसके उलट यह भी ठोस बिन्दु है कि कोई भी गिरोह हजार-दो हजार फोन/डिवाइस से अधिक तो क्या ला पाएगा? तत्काल पहचाने और पकड़े जाएंगे सारे के सारे। उनकी साजिश ही उनकी गिरफ्तारी का कारण बन जाएगी। क्योंकि कितनी लोकेशन बदलेंगे?
दूसरा, कि व्हॉट्सएप अभी ग्रुप को देखकर ही ढेर सारे उपाय कर रहा है। सरकारें भी ग्रुप मैसेजिंग पर ध्यान दे रही हैं। जबकि तथ्य और दृश्य सिद्ध कर रहे हैं कि अधिक तबाही वन-टू-वन मैसेजिंग से हो रही है। जैसे, 9 राज्यों की लिंचिंग घटनाएं देखें – तो कही भी भीड़ सात सौ-आठ सौ से कम लोगों की नहीं थी। कहीं-कहीं तो ये साढ़े तीन-चार हजार उन्मादियों से भरी थी।
व्हाॅट्सएप ग्रुप 256 से अधिक का नहीं होता। इतने लोगों को, जाहिर है निजी मैसेज ही किए गए होंगे। फिर, ख़ुद व्हॉट्सएप ने बताया है कि केवल 25% लोग ही ग्रुप में हैं। बाकी लगभग 15-18 करोड़ तो ग्रुप में हैं ही नहीं। फेसबुक की इस कंपनी ने यह भी बताया है कि प्रत्येक 10 व्हॉट्सएप मैसेज में से 9 निजी, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर को सीधे भेजे गए होते हैं। तो, व्हॉट्सएप से सरकार को जो सुरक्षा उपाय चाहिए – वो वास्तव में वन-टू-वन मैसेजिंग पर चाहिए।
जो संभव भी है।
बस, अभी सीमित है। सभी ओर नहीं। जैसे, सबसे जरूरी उपाय है, ‘फॉरवर्ड’ लेबल के साथ ‘माय ओन मैसेज’ जैसा लेबल। यानी, पूर्ण जिम्मेदारी। और कानून इसे अभी इन्वेस्टीगेशन का सर्वाधिक उपयोगी व ठोस तरीका मानता है। तो इसे कानूनन, कोर्ट में भी एडमिसिबल एविडेन्स बनाना आवश्यक है। जो अभी हमारे देश में कम प्रचलित है – वो व्हॉट्सएप का सहयोगी बन गया है। काफी कारगर हो सकता है अफवाह, झूठ और बरगलाने-भड़काने वाली आपराधिक सामग्री को जांचने-पहचानने में। वो है फैक्ट चैकर बूमलाइव। व्हॉट्सएप ने कर्नाटक चुनाव के समय उसका साथ किया था।
धीरे-धीरे, काफी कुछ नियंत्रित हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में धुले में 5 की हत्या के बाद, तत्काल वैसी ही भीड़ ने मालेगांव में कुछ लोगों को बंदी बना लिया था। उसी तरह के ‘बच्चों के अपहरण करने वाले गिरोह’ के संदेह में। बूमलाइव ने तत्काल दो ऐसे वीडियो पकड़े – जो महाराष्ट्र की घटना से पूरी तरह असंबद्ध, अलग थे। एक कर्नाटक का था। किसी बच्चे को अगवा करने से संबंधित था ही नहीं। किन्तु बहकावे के लिए वो चलाए-भेजे जा रहे थे।
सुरक्षा को लेकर व्हाॅट्सएप का रवैया अलग होते हुए भी अपराध रोकने में पुलिस उसे सहयोगी बना सकती है। अभी कंपनी यह दावा करती है कि वो एंड-टू-एंड इन्क्रिप्शन देती है। यानी भेजने वाले या पाने वाले के अलावा वो मैसेज/कंटेन्ट किसी के पास नहीं जा सकता। ख़ुद व्हॉट्सएप कंपनी के पास भी नहीं। ये पूर्ण सत्य नहीं है।
जो मैसेज भेजे जा चुके हैं, डिलीवर्ड हैं – वे तो व्हॉट्सएप सर्वर पर भी नहीं है – यह सच है। किन्तु जो प्राप्त नहीं हुए हैं – वो उनके सर्वर पर एक तय समय तक बने रहते हैं। यानी देखे जा सकते हैं। और उनका मेटाडेटा? यानी समूचे डेटा पर डेटा या का डेटा। वो तो हमेशा है। कभी मिटेगा नहीं। अपराध पकड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम, सशक्त और सरल उपाय। बशर्ते, कानून के रखवाले चाहें।
क्योंकि अभी तो देश के बड़े हिस्से में कानून के रखवाले यही मानते हैं कि सोशल मीडिया में सर्वाधिक आसान, लोकप्रिय व्हॉट्सएप का डेटा पकड़ा नहीं जा सकता। किन्तु, यह तो केवल हत्यारी भीड़ और व्हॉट्सएप दोनों की पहचान न होने के कारण निकली चर्चा है। वास्तव में तो गुप्तचर व्यवस्था देश में पूर्णत: विफल है।
वरना, एक के बाद एक हो रहीं भीड़ द्वारा हत्याओं के ट्रेंड को कोई पकड़ क्यों नहीं पाया? इतनी व्यवस्था बनने के बावजूद खुफ़िया पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाता? पहले गौरक्षकों की उन्मादी भीड़ चल रही थी। अभी इतना सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, तब भी हापुड़ में क्या हुआ? और गौरक्षकों के बाद अब ये बच्चों के अपहरण करने वालों के गिरोह पर अफ़वाहें। और आक्रोशित जनसमूह।
राज्यों की जिम्मेदारी तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ‘कारण’ नहीं सुनेंगे। हिंसा, हिंसा है। भीड़ की हिंसा का कौनसा कानून है – यह कुछ नहीं सुनेेंगे। हिंसा रोकनी ही होगी। इसे व्यावहारिक रूप से देखें तो लौटकर ख़ुफिया तंत्र पर ही आ जाएगा। ‘बीट स्तर’ पर ख़ुफिया तंत्र ही काम करता है। उसे न कोई बड़े भंडाफोड़ पर प्रशंसा मिल रही है – न ही भारी चूक होने पर प्रताड़ना।
चूंकि सभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं, व्हॉट्सएप पर दो-दो महीनों से धीरे-धीरे चलाए जा रही सामग्रियों से भड़क कर हुईं – तो वो ख़ुफिया पुलिस ही क्या जिसे इतने बड़े स्थानीय सार्वजनिक ट्रेंड का पता तक न चले? अब केन्द्रीय गृह मंत्रालय से लेकर देशभर की सरकारें व पुलिस मुस्तैद हो गई है।
सारी भारतीय कानून-व्यवस्था अपराध हो जाने की प्रतीक्षा करती रहती है। प्रिवेन्टिव नहीं है। अपराध रोकने के लिए वर्दीधारी व्यवस्था के पास कुछ भी नहीं है। अधिकार भी नहीं। इसलिए, ऐसे में गुप्तचर पुलिस की महत्ता सर्वाधिक है। साइबर पुलिस का योगदान सर्वाधिक हो सकता है। क्योंकि गुप्तचर व साइबर पुलिस अपराध की आहट पा लेते हैं। इनका काम ही अपराध को घटने से पहले ही पकड़ना है।
इनके लिए तो सोशल मीडिया ट्रेन्ड और सहायक है – चूंकि पहले से ही पता चल सकता है। उन्मादी भीड़ रुके, असंभव है। किन्तु रोकनी ही होगी। व्हाॅट्सएप पर अापराधिक सामग्री रुके, असंभव है। किन्तु रोकनी ही होगी। कोई भी भीड़ समझाने से नहीं, बल से ही रुकती है।
कश्मीर उदाहरण है। न रोकने से क्या हुआ। कोई भी कंपनी मुनाफ़े के लिए ही बनी है। यदि किसी कंपनी की हठधर्मिता, अपराधियों को बढ़ावा देती है – तो सरकार बताए कि राजहठ के समक्ष सब हठ फीके हैं। देश के ही हाथ में होना चाहिए कि कंपनियां देशवासियों के हित में कितना-कैसा-कहां व्यापार करें। देश भीड़ नहीं है। न ही देशवासी भीड़ से मरने वाले।
कल्पेश याग्निक का कॉलम : (साभार : दैनिक भास्कर.कॉम)